दहेज प्रथा: भारत में एक गंभीर सामाजिक समस्या का इतिहास और वर्तमान
दहेज प्रथा का इतिहास
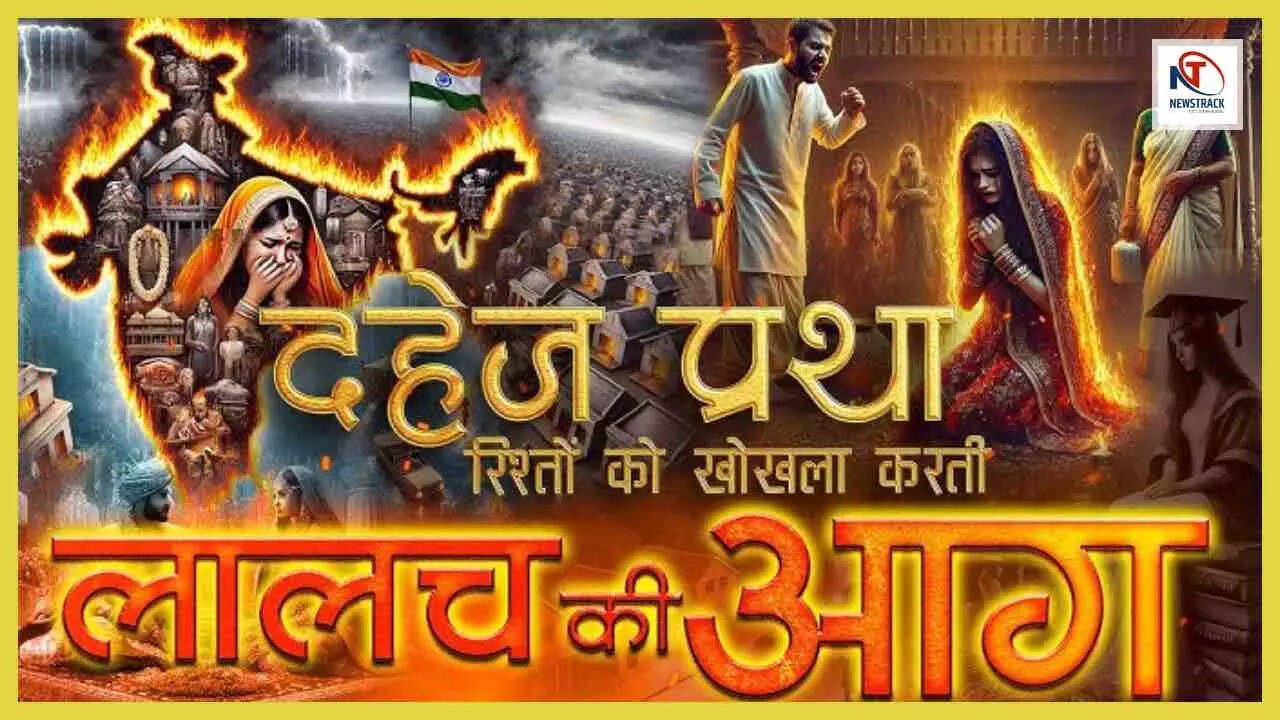
दहेज प्रथा का इतिहास (फोटो - सोशल मीडिया)
दहेज प्रथा का इतिहास: भारत, जो सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं से भरा हुआ है, में विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं होता, बल्कि यह दो परिवारों के बीच एक महत्वपूर्ण सामाजिक बंधन होता है। सदियों से यह वैवाहिक परंपरा धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ निभाई जाती रही है। लेकिन इस व्यवस्था में एक ऐसी प्रथा भी शामिल हो गई है, जिसने समय के साथ गंभीर सामाजिक संकट का रूप ले लिया है, जिसे हम दहेज प्रथा के नाम से जानते हैं।
दहेज का अर्थ है विवाह के समय वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली धन-संपत्ति, वस्तुएं, गहने, भूमि या अन्य बहुमूल्य उपहार। यह प्रथा कभी सहयोग और प्रेम की भावना से शुरू हुई थी, लेकिन अब यह लालच और सामाजिक दिखावे की एक खतरनाक दौड़ में बदल गई है। आज यह एक ऐसी कुप्रथा बन चुकी है, जिसके कारण अनगिनत महिलाएं शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं, और कई मामलों में तो उनकी जान भी जा रही है।
इस लेख में हम दहेज प्रथा के उद्भव, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, बदलते स्वरूप और इसके वर्तमान सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करेंगे।
दहेज प्रथा का प्रारंभिक इतिहास
दहेज प्रथा का प्रारंभिक इतिहास

दहेज प्रथा की जड़ें भारतीय समाज में गहरी और प्राचीन हैं। यह प्रथा नई नहीं है, बल्कि इसके मूल तत्व वैदिक काल से जुड़े हुए हैं। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि प्राचीन भारत में दहेज का स्वरूप आज के लालची और शोषणकारी रूप से बिल्कुल भिन्न था।
वैदिक काल (1500–500 ई.पू.) में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था। उस समय दहेज को ‘स्त्रीधन’ कहा जाता था, जो माता-पिता द्वारा अपनी बेटी को उसकी नई जिंदगी के लिए दिया जाने वाला एक प्रकार का संरक्षण था। इसमें वस्त्र, आभूषण, आवश्यक वस्तुएं, भूमि या कभी-कभी गाय-बैल तक शामिल होते थे। यह धन या सामग्री वर पक्ष को नहीं, बल्कि वधू को व्यक्तिगत रूप से दिया जाता था, और इसे उसकी निजी संपत्ति माना जाता था।
उदाहरण के लिए, ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ जैसे ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि राजा जनक ने सीता के विवाह में उपहार दिए, जो सम्मान स्वरूप थे, कोई अनिवार्य शर्त नहीं।
स्त्रीधन का महत्व - प्राचीन समय में स्त्रीधन का उद्देश्य महिला को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना था। चूंकि उस समय महिलाएं अक्सर घरेलू भूमिकाओं में सीमित रहती थीं, इसलिए यह धन उनके अधिकार का प्रतीक होता था, जिसे न तो पति और न ही ससुराल वाले छीन सकते थे। हिन्दू धर्म के धर्मशास्त्रों जैसे मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी स्त्रीधन को सुरक्षित रखने की बात कही गई है।
मध्यकाल में परिवर्तन
समय के साथ जैसे-जैसे समाज में जाति व्यवस्था, पितृसत्ता और भौतिक लालच की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, दहेज का स्वरूप भी विकृत होने लगा। मध्यकाल (लगभग 1200–1800 ई.) में जब भारत पर बाहरी आक्रमणकारियों का प्रभाव बढ़ा, और राजनैतिक अस्थिरता फैली, तब लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सामाजिक चिंताएं भी बढ़ीं।
इसके कारण विवाह में दहेज एक अनिवार्य शर्त की तरह देखा जाने लगा, ऐसा माना जाने लगा कि अधिक दहेज देने से बेटी की ससुराल में स्थिति मजबूत होगी। धीरे-धीरे यह मानसिकता घर कर गई कि वर पक्ष को संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक उपहार देना आवश्यक है।
ब्रिटिश काल में दहेज प्रथा का संस्थागत रूप
ब्रिटिश शासन के दौरान कई सामाजिक व्यवस्थाएं और कानूनी संरचनाएं बदलीं। हिंदू उत्तराधिकार कानून ने महिलाओं के अधिकारों को सीमित कर दिया और स्त्रीधन की वैधता पर भी प्रभाव डाला। इससे वधू के पास उसकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार कम होने लगा और ससुराल वालों द्वारा उसे हड़पने की घटनाएं बढ़ीं। इसी दौरान दहेज एक सामाजिक दिखावे और प्रतिष्ठा का विषय बनता गया। अब यह केवल बेटी को कुछ देने की भावना न रहकर, वर पक्ष की माँगों को पूरा करने की प्रक्रिया बन गई।
स्वतंत्र भारत और दहेज प्रथा
1947 में भारत आज़ाद हुआ, और 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार दिए गए। लेकिन सामाजिक सोच इतनी जल्दी नहीं बदली। आज़ादी के बाद भी दहेज प्रथा पहले की तरह चलती रही और कई मामलों में और भी विकराल हो गई।
1950 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक भारत में दहेज को लेकर होने वाले उत्पीड़न और दहेज हत्याओं की संख्या बढ़ने लगी। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने दहेज को कानूनी रूप से अपराध घोषित किया।
कानून बनाम हकीकत
कानून बनाम हकीकत

भारत सरकार ने दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कई कानूनी कदम उठाए। उनमें सबसे प्रमुख हैं:
दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961) - यह कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि विवाह के पहले, दौरान या बाद में वर या उसके परिवार द्वारा दहेज की मांग करना या देना-दिलवाना अपराध है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 498A - इसके तहत यदि विवाहिता महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, तो पति और उसके परिवार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।
धारा 304B (दहेज मृत्यु) - यदि विवाह के सात वर्षों के भीतर महिला की मृत्यु होती है और वह दहेज के कारण उत्पीड़न का शिकार रही है, तो इसे "दहेज मृत्यु" माना जाता है, और सख्त सजा का प्रावधान है।
NCRB के आंकड़ों में दहेज हत्या की भयावह तस्वीर
NCRB के आंकड़ों में दहेज हत्या की भयावह तस्वीर

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार, भारत में हर वर्ष हजारों महिलाएं दहेज के कारण अपनी जान गंवा देती हैं। वर्ष 2017 में कुल 7,466 मामले दर्ज किए गए, जो 2018 में घटकर 7,167 रह गए। इसके बाद 2019 में यह संख्या 7,141 रही, जबकि 2020 में यह मामूली रूप से घटकर 6,966 पर आ गई। वर्ष 2021 में दहेज हत्या के कुल 6,589 मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि दहेज हत्या की घटनाएं धीरे-धीरे घट रही हैं, लेकिन संख्या अभी भी चिंताजनक रूप से अधिक है।
यह ध्यान देने योग्य है कि ये आंकड़े केवल उन्हीं मामलों को दर्शाते हैं जो पुलिस में दर्ज किए गए हैं। सामाजिक शर्म, परिवार का दबाव, और कानूनी प्रक्रिया की जटिलता के कारण कई पीड़िताएं सामने नहीं आ पातीं, जिससे असल संख्या इन आंकड़ों से कहीं अधिक हो सकती है। दहेज हत्या भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत दर्ज की जाती है, और यह कानून 7 वर्षों के भीतर हुई विवाहिता की संदेहास्पद मृत्यु को ध्यान में रखता है, बशर्ते उससे पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो।
इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में दहेज प्रथा अब भी एक गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है। इसे केवल कानून से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, शिक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण के ज़रिए ही समाप्त किया जा सकता है।
स्वतंत्र भारत में दहेज से जुड़ी प्रसिद्ध घटनाएँ
स्वतंत्र भारत में दहेज से जुड़ी प्रसिद्ध घटनाएँ

निर्मला हत्याकांड (1980) - उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की यह घटना भारत भर में चर्चा का विषय बनी। निर्मला नामक एक शिक्षित युवती की शादी एक सरकारी कर्मचारी से हुई थी। वर पक्ष ने विवाह के बाद स्कूटर और फ्रिज की मांग की। जब यह पूरी नहीं हुई, तो निर्मला को प्रताड़ित किया गया और अंततः जला कर मार डाला गया। इस मामले ने पूरे देश में आक्रोश फैलाया और दहेज कानूनों की माँग को बल मिला।
सुषमा शर्मा केस (1995, दिल्ली) - सुषमा, एक इंजीनियरिंग ग्रैजुएट, की शादी एक डॉक्टर से हुई थी। विवाह के बाद लगातार दहेज की मांग की जाती रही। कई शिकायतों के बाद भी पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। अंततः उसे मानसिक और शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। यह केस दिल्ली हाई कोर्ट तक गया और इसके निर्णय के बाद IPC की धारा 498A को और मजबूत बनाया गया।
सामाजिक जागरूकता से उपजी घटनाएँ
सामाजिक जागरूकता से उपजी घटनाएँ
"सात फेरों का संकल्प" - बिहार (2018) - बिहार के औरंगाबाद जिले में एक गांव की युवती नीलम देवी ने विवाह के समय वर पक्ष द्वारा अचानक मोटरसाइकिल की मांग करने पर शादी से इनकार कर दिया। उसने पूरे समाज के सामने यह कदम उठाया और कहा कि “जिस शादी में सम्मान न हो, वह शादी नहीं बंधन होती है।” इस साहसिक कदम की पूरे देश में सराहना हुई।
दहेज के कारण प्रसिद्ध आत्महत्याएँ और हत्याएँ
दहेज के कारण प्रसिद्ध आत्महत्याएँ और हत्याएँ

अनामिका की कहानी (2010, मध्य प्रदेश) - अनामिका एक होनहार स्नातक थी। उसकी शादी एक बैंक कर्मचारी से हुई थी। शादी के बाद एक कार और 2 लाख रुपये की मांग की गई। जब उसका परिवार यह पूरी नहीं कर सका, तो उसे आए दिन मारपीट और अपमान झेलना पड़ा। एक दिन जब वह अपने मायके आई तो उसने आत्महत्या कर ली, और एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें वर पक्ष की क्रूरता का वर्णन था। यह मामला कई महीनों तक मीडिया में छाया रहा।
वर्तमान समय में दहेज प्रथा के दुष्परिणाम
वर्तमान समय में दहेज प्रथा के दुष्परिणाम
वर्तमान समय में दहेज प्रथा समाज में अनेक भयावह दुष्परिणाम लेकर आई है, जिनमें सबसे गंभीर महिलाओं पर होने वाला मानसिक और शारीरिक अत्याचार है। आज भी कई महिलाएं अपने ससुराल में केवल इस कारण प्रताड़ना झेल रही हैं क्योंकि उनके माता-पिता दहेज की 'उचित' राशि या वस्तुएं नहीं दे पाए। यह प्रताड़ना केवल मारपीट तक सीमित नहीं होती, बल्कि मानसिक उत्पीड़न और सामाजिक अपमान तक फैली होती है। इसके अलावा, दहेज हत्याएं एक अत्यंत दुखद और चिंताजनक पहलू हैं। हर साल हजारों महिलाएं दहेज के कारण मारी जाती हैं या लगातार हो रहे उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, भारत में हर दिन औसतन 20 से अधिक महिलाएं दहेज की बलि चढ़ जाती हैं, जो समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। इसके साथ ही, दहेज की मानसिकता के कारण लड़कियों को अब भी कई परिवारों में बोझ समझा जाता है, जिससे बेटा-बेटी में भेदभाव बढ़ता है। यह सोच न केवल महिला सशक्तिकरण के रास्ते में रुकावट है, बल्कि समाज के संतुलन और नैतिक मूल्यों को भी कमजोर करती है।
समाधान की दिशा में कदम
समाधान की दिशा में कदम
जनजागरण और शिक्षा - लोगों को यह समझाना होगा कि विवाह कोई लेन-देन नहीं, बल्कि सहयोग और समर्पण का रिश्ता है।
कानून का कड़ाई से पालन - दहेज लेने और देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
महिला सशक्तिकरण - जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी, तो वे न केवल दहेज मांगने वालों का विरोध कर पाएंगी, बल्कि अपने अधिकारों के लिए आवाज भी उठा सकेंगी।
दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा - समाज में ऐसे उदाहरण स्थापित करने होंगे जहाँ बिना दहेज के विवाह हों, और उन्हें सम्मानित किया जाए।
मीडिया और फिल्मों में सच्ची घटनाओं पर आधारित चित्रण
मीडिया और फिल्मों में सच्ची घटनाओं पर आधारित चित्रण
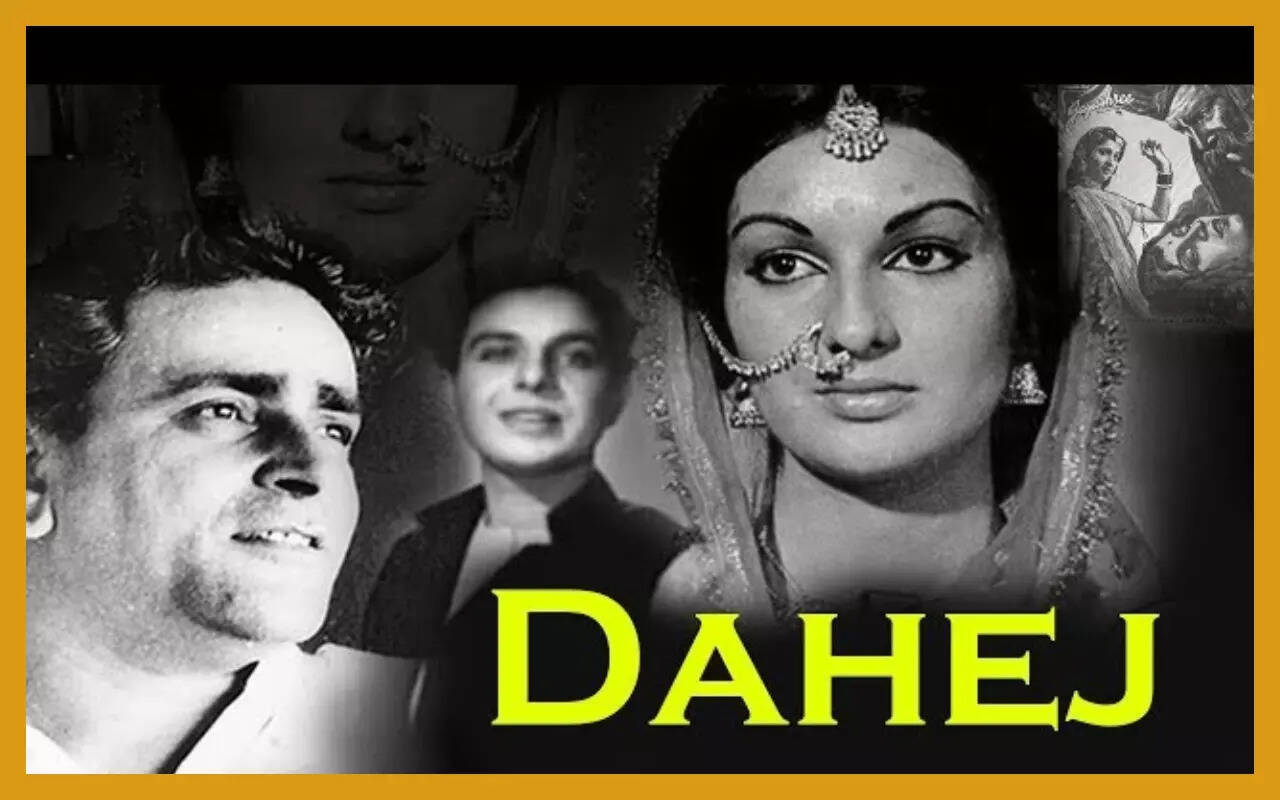
.png)